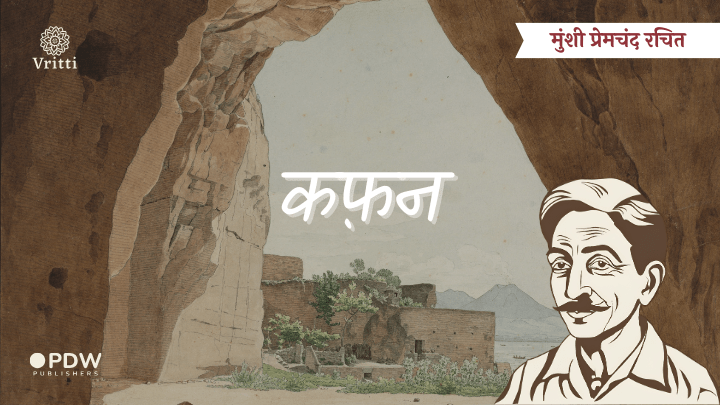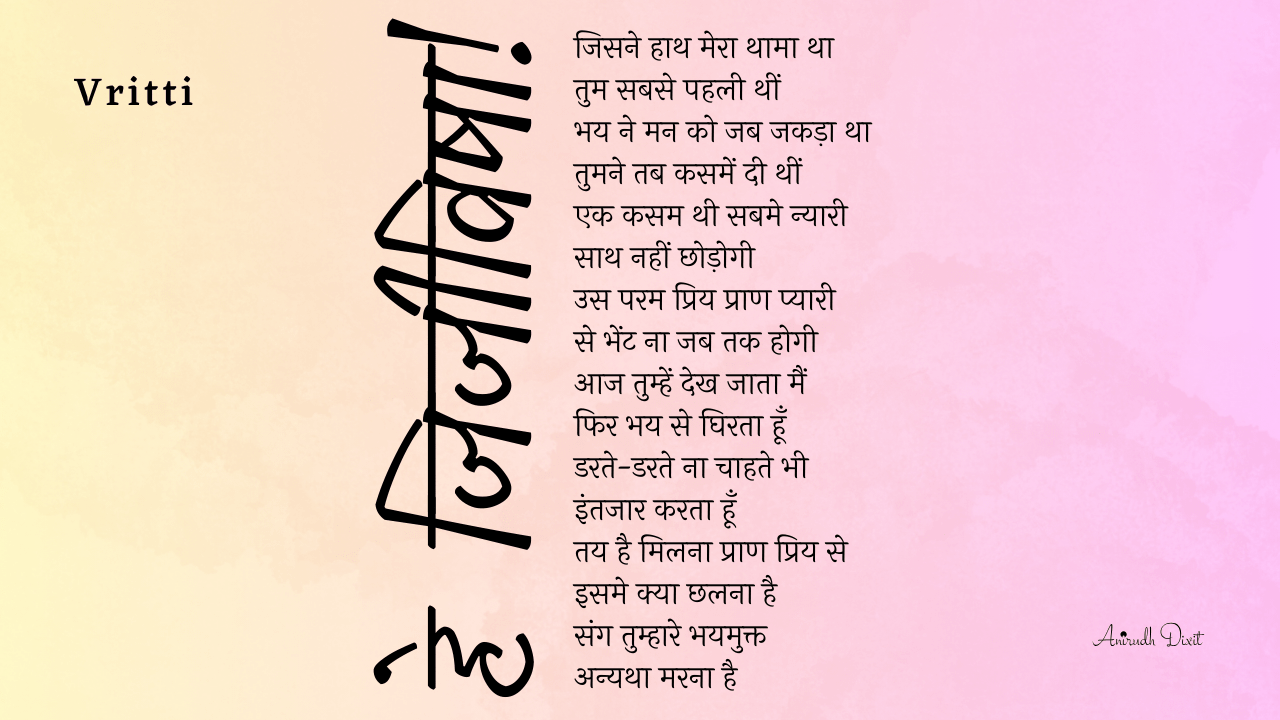About Story and Author
Table of Contents
About ‘Nitya Anitya’ by Anirudh Dixit
In “Nitya Anitya,” Anirudh Dixit weaves a compelling narrative that explores the intricate dance between fate and free will. Set against the backdrop of a college library, this poignant story follows Anirudh, a law student, as he navigates his emotional landscape filled with the remnants of a past relationship and the allure of a new connection.
The story opens with Anirudh grappling with existential questions about destiny: Are our lives preordained, or do we carve our own paths? His introspective journey takes a transformative turn when he encounters Nitya, a spirited and enigmatic young woman. Their initial interactions spark a series of contemplative dialogues that challenge Anirudh’s views on love, relationships, and the very essence of existence.
As Anirudh and Nitya’s friendship blossoms, readers are drawn into a rich tapestry of emotions, philosophical musings, and relatable experiences. The story deftly illustrates the tension between the comfort of solitude and the thrill of human connection, making it a relatable read for anyone who has pondered their place in the world.
“Nitya Anitya” explores themes of fate, choice, and self-discovery, prompting readers to reflect on their life decisions and the nature of love. This contemporary fiction piece blends romance with philosophical introspection, appealing to those who enjoy thought-provoking literature.
If you seek a narrative that challenges your views on fate while celebrating emerging love, “Nitya Anitya” is a must-read. Join Anirudh on his journey of self-discovery and uncover insights into your own life. Dive into this captivating tale and explore the delicate balance between destiny and choice.
About Anirudh Dixit
Anirudh Dixit is a contemporary author known for his engaging storytelling that explores themes of love, fate, and self-discovery. With a background in law, he blends emotional depth with philosophical insight, creating relatable narratives that resonate with readers of all ages.
प्रस्तावना
मानव सभ्यता प्राचीनकाल से प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगी हुयी है। प्रयासरत सभी को कुछ ना कुछ अमूल्य अवश्य मिला है। किन्तु हर उत्तर अपने साथ एक प्रश्न अवश्य लाता है। हम चाहें जितने उत्तर खोज लें कोई ना कोई प्रश्न सदैव हमे परेशान कर रहा होता है।
इसी प्रकार एक बहुचर्चित प्रश्न है – “भाग्य”। क्या भाग्य होता है? क्या इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। क्या किस्मत ही सब कुछ है? अब यदि मैं इस प्रस्तावना के माध्यम से उत्तर देने बैठा तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप या तो तर्क-वितर्क में व्यस्त हो जाएंगे या कुछ ही देर में नींद के झोंके लेने लगेंगे। और फ़िलहाल मैं ये दोनों ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि भाग्य का प्रश्न एक वाक्य में तो बस इतना ही है कि “मेरे द्वारे लिए गए फ़ैसले पहले से तय थे या नहीं।”
अब क्योंकि भाग्य पर चर्चा शुरू हो ही गयी है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बाकी रही बात भाग्य की तो वह आप स्वयं तय कीजियेगा…
कहानी – नित्य अनित्य
☘☘☘
“क्या सागर जनता है कि वह सागर है? क्या नदी जानती है कि वह नदी है? यदि नहीं, तो सागर क्यों नदी नहीं बन जाता? क्यों अपनी सीमायें तोड़कर अपनी चंचलता को प्रकट नहीं कर देता? क्या वह केवल इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि वह सागर का स्वभाव नहीं है? नदी में वेग है; सागर में ठहराव है। दोनों अपने-अपने स्वभाव को दर्शाते हैं। किन्तु स्वभाव? स्वभाव कैसे तय होता है? क्या सागर ने अपना स्वभाव खुद चुना है? नहीं, कदापि नहीं। कोई आपना स्वभाव स्वयं कैसे चुन सकता है और क्या चयन शक्ति किसी के पास सच में होती भी है?” मैं लिखते-लिखते रुक गया। अचानक आयी हलकी-हलकी सुगंध ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने एक नज़र उस ओर देखा। एक युवती पुस्तकालय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रही थी। मैं फिर नदी और सागर में व्यस्त हो गया।
एल.एल.बी. की तीसरी छमाई की परीक्षा समाप्त होते ही मैंने पुस्तकालय से जुड़ने का फैसला कर लिया था। अब और किसी अप्सरा के लिए अपनी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था। अब तक जो हुआ सो हुआ। बाईस जनवरी, दो हज़ार तेईस, हाँ, बीस को परीक्षा समाप्त हुई थी और बाईस को मैंने पुस्तकालय जाना शुरू किया था। वे दिन काफी अजीब थे या कहूं की मैं ही काफ़ी अजीब हो गया था। किसी से मिलने की इच्छा नहीं हुआ करती थी बल्कि सबसे दूर-दूर रहने का मन होता था। ऐसा लगता था जाने क्यों ही भेज दिया गया हूँ इस धरती पर। तिशा के साथ बीते हुए लम्हों को याद करना सुखदायी होता था अन्यथा सबकुछ रसहीन। जीवन बेरंग-सा प्रतीत होने लगा था। जबसे तिशा के बारे में लिखा था। मेरे प्रति लोगों का नज़रिया ही बदल गया था। कोटि-कोटि परामर्श मिलने लगे थे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। सच कहूं तो “जितने मुँह उतनी बातों” का अर्थ मुझे तब ही समझ आया और “जिस पर बीतती है वही जनता है” का भी। आख़िर, इस सबसे बचने के लिए ही तो पुस्तकालय जाना शुरू भी किया था।
‘पुस्तकालय’ यानि पुस्तकों-किताबों का घर। पुस्तकालय में सभी को शांत रहने के निर्देश दिए जाते हैं, सिवाय पुस्तकों के। यहाँ केवल पुस्तकों को बोलने की आज़ादी होती है। मुझे अपने लिए यह सबसे शानदार जगह लगी। मुझे सिर्फ लोगों के बोलने से परेशानी थी, किताबों के बोलने से नहीं। मैंने दैनिक रूप से पुस्तकालय जाना प्रारम्भ किया। वहाँ जाकर में पुस्तकों में खो जाया करता था। अलग-अलग विचारों पर विपरीत विचारकों के मतों को पढ़ना और उनसे सहमत-असहमत होना एक आदत-सी बन गयी थी। किताबों में यदि कोई सूत्र वाक्य मिलता तो उसे रेखांकित कर देता। इस प्रकार रेखांकित करने से विभिन्न विचारों की टकराहट का आनंद लिया जा सकता था। वह कार्य सत्य ही काफी आकर्षक था। कई बार ऐसा होता है कि कोई सूत्र वाक्य आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। आप अक्सर सोचते-सोचते शून्य में खो जाते हैं। घंटो किसी एक जगह नज़र टिक जाती है, तब ना तो कुछ सुनाई देता है ना दिखाई। केवल विचार होते है, ना आप होते हैं न यह संसार, केवल विचार।
मुझे अब भी ध्यान है वह पांच फरवरी की बात है। मौसम काफ़ी खुशनुमा था। सर्दियों का कहर काफी हद तक कम हो गया था। सुबह के तकरीबन ग्यारह बजे थे। पुस्तकालय पहुँचने में थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो गया था परन्तु मुझे कोई खास चिंता नहीं थी। मैं हल्का-सा दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसा। जैसा आशंकित था वही हुआ, दरवाज़ा खुलने पर आज किसी ने घूरा नहीं। रविवार के दिन पुस्तकालय आने का यही लाभ है इस दिन पुस्तकें होती हैं और मैं। संतुष्टि के साथ मैंने पुस्तक उठाई और अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गया। किताब मेज़ पर रखकर एक नज़र पुस्तकालय को देखा। हर तरफ कुछ जाना पहचाना सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने किताब खोली और शब्दों को निहारना शुरू किया। कुछ ही देर में, मैं इस शांत, अकेले भवन से निकल चुका था।
“हेलो! क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो?” एक बहुत ही प्यारी पर गुस्से से भरी हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।
मैंने हड़बड़ाहट में ऊपर की ओर देखकर कहा – ” जी, फरमाइए।”
मेरे सामने एक पांच फुट और चार या पांच इंच लम्बी लड़की नाक पर गुस्सा लिए खड़ी थी। उसका चेहरा गोल था और रंग गेंहुआ रहा होगा। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें मुझे डराने के लिए काफी थीं।
“मुझे आप बता सकते हैं कि ‘महाभोज’ कहाँ मिलेगी?” हाँलाकि उसके चेहरे पर अब भी लालिमा थी परन्तु इस बार आवाज़ में कुछ नरमी थी।
“मन्नू भंडारी?”
“जी, वही।”
“यह लीजिये, यह मेरे ही पास है।” मैंने उपन्यास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा।
“अगर आप पढ़ रहे हैं तो रहने दीजिये, मैं कुछ और देख लुंगी।” उसने पीछे हटते हुए कहा।
“मैं बस अंत पर ही हूँ, दस मिनटों में आप तक पहुंचा दूंगा तब तक चाहो तो ‘यही सच है’ पढ़ लीजिये” मैंने नटखटपन में मुस्कुराकर कहा।
“पढ़ी है।” आशय भांपते हुए लम्बी सी मुस्कान के साथ उसने कहा।
हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का-सा मुस्कुराये और अपने-अपने कार्यों में संलग्न हो गए। आखिर कुछ ही मिनटों में बिसू से चली आ रही दुर्निवार सम्मोहन-भरी खतरनाक लपकती अग्नि-लीक बिन्दा से होते हुए सक्सेना तक पहुँच गयी। मैंने सामने की ओर देखा। वह काफी ध्यान से अखबार पढ़ रही थी, मैंने टोंकना उचित नहीं समझा इसलिए किताब को धीरे से उसकी ओर सरका दिया। मैं अभी अपना हाथ पीछे खींच ही पाया था कि उसने कहा –
” थैंक्स ! वैसे आप संडे को भी लाइब्रेरी आये हैं आपका भी एग्जाम है क्या?”
“नहीं। तुम्हारा है क्या?”
“नहीं, पर अक्सर केवल वही लोग संडे को लाइब्रेरी आते हैं या तो जिनका घर पर मन नहीं लगता या उनका एग्जाम होता है। आप कौनसी केटेगरी से हो?” अपनी भोंहो को शरारती रूप से मटकाकर उसने पूछा।
“ऑब्वियस्ली, पहली वाली।” मैंने खिलखिलाते हुए उत्तर दिया।
वह मेरी ओर देखकर हल्का मुस्कुराई और किताब खोलकर पढ़ने में मगन हो गई। मैं उसकी और बड़े गौर से देख रहा था। वैफरेर ग्लासेज़ के डिज़ाइन का उसका चश्मा उसके चेहरे को अत्यधिक आकर्षक एवं संजीदा बना रहा था। मेरा मन और आंखें मानो दोनों ही सलाह करके उसके रूप का रसपान करने में लगे हुए थे। और जिस बात की आशंका थी, वही हुआ। उसने पलकें उठाकर मेरी और देखा। मुझे कुछ ना सूझा। मैंने सकपकाकर प्रश्न किया – “उस दिन आपने कौन सा परफ्यूम लगाया था?”
“किस दिन?” उसके चेहरे पर आए हुए असुविधाजनक भाव एकाएक विस्मय में परिवर्तित हो गए।
मैं तब तक संभाल गया था। मैंने कहा – “उस दिन जब आप रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रही थीं, वह शायद आपका पहला दिन था।”
“ओह… अच्छा। उस दिन… अगर तुम भी उसी दिन की बात कर रहे हो, तब तो बस मैं जॉइन करने आई थी। मैनली तो मुझे बाहर जाना था। सो, आई वॉज़ वेअरिंग ‘प्रिस्टीन’ ‘स्किन’। डिड यू लाइक डेट?”
“ऑफकोर्स…टाइटन ना”
“यप, थैंक्स।” उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और फिर किताब में मग्न हो गई।
मैं जो अब तक किसी से बात करना नहीं चाहता था और किताबों के सिवाय किसी का बोलना पसंद नहीं कर रहा था। मेरा मन अब किताबों में नहीं लग रहा था। मन में अलग-अलग बातें चल रही थी। “बाइस – तेईस की होगी। लग तो टॉपर रही है। पता नहीं हिंदू है या मुसलमान। खैर जो भी हो मुझे क्या? नाम क्या बताया था? नाम तो पूछ ही लेना चाहिए।” फिर मैंने मन ही मन रिहर्सल करना शुरू किया। “वैसे आपका नाम क्या है?” अरे, नहीं ऐसे नहीं। “मैं अनिरुद्ध और आप?” ना…ना…फोकस…शांत…किताब से बात शुरू करता हूं…पर किताब से क्या ही बात शुरू करूं…हूँ…, परफ्यूम की बात आगे बड़ाई जाय…पर अब क्या ‘टाटा’ तक ले जाऊं…ओह। भला मेरे लिए बात करना इतना मुश्किल कब से हो गया?…ओके …लेट्स कीप इट सिंपल…।
“अपने नाम क्या बताया अपना? आई मीन योर गुड नेम?” मुझसे साधारण नाम नहीं पूछा जा रहा और मम्मी मेरी इसी ज़बान को कैंची की तरह तेज़ बताती हैं।
“नित्या। आपका?” फिर एक बार उसी धैर्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने मेरी और देखते हुए उत्तर दिया।
“अनिरुद्ध। आप पढ़ाई कर रही हैं?”
कई बार लोग मेरी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं बोलता अच्छा हूं। किंतु इस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं बोलना भूल गया हूं या वह सब झूठे हैं। मुझे तब समझ में आया क्यों अपने मित्रों द्वारा की गई तारीफ को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
“हाँ और आप?”
उसके उत्तर सूखे और रसहीन प्रतीत हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उसे परेशान कर रहा हूं।
“हाँ, एल. एल. बी. सेकंड ईयर चल रहा है।”
“लॉ… गुड।” उसने इतना कहा और फिर किताब पढ़ने में मग्न हो गई।
मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। अरमानों का गला घोंटने के सिवाय कोई विकल्प शेष न था। मैंने उसकी ओर से ध्यान हटाकर किताब में लगाना ही उचित समझा। वैसे नाम अच्छा है। नित्या…बंद आंखों के साथ एक ठंडी आह निकाली और मैं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। पता नहीं कहाँ था? फिर होश में आया और किताब पढ़ने लगा। इस बार ध्यान नहीं भटका। मन शांत हो चुका था।
तकरीबन 3:00 बजे होंगे। में अभी सेगल नगरी में ही विचरण कर रहा था। नित्या ने कुर्सी से उठते हुए पूछा – “आप अभी और रुकेंगे?”
“हाँ, अभी दो-चार पन्ने और पलटने हैं।” मैंने नींद भरी आंखों से उसकी और देखते हुए कहा।
“ओके… मिलकर अच्छा लगा।” कहते हुए वह बाहर की ओर निकल गई।
मैं निस्तब्ध अब भी दरवाजे की ओर देख रहा था। मैं देख पा रहा था उम्मीदों को फिर जागते हुए। मन फिर मचलने लगा था। “नित्या…आपका?…मिलकर अच्छा लगा।” मेरे चेहरे पर धीरे-धीरे मुस्कुराहट आने लगी। एक अरसे बाद मन इतना हल्का महसूस कर रहा था। मैं उठकर घर की ओर चल दिया।
रास्ते भर भावनाएं हिचकोले खाती रही। मन में बहार आई हुई थी। हवाओं सा बहते हुए घर पहुँचा।
“जय श्री कृष्ण! माँ।” आज आवाज में अलग ही चहचाहक थी।
माँ ने भाँप लिया था। नटखटी मुस्कान के साथ बोलीं।
“जय श्री कृष्ण। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो गुल से बात हो गई लगता है?”
“गुल” कुछ मीठे जख्म हरे हो गए। मैंने खुद को संभालते हुए और नाटकीय ढंग से खीझते हुए कहा – “छोड़ो गुल को।”
“अच्छा जी, अब छोड़ो और तब पूरा दिन फ़ोन पर हाय गुल कैसी हो।”
“आज पता है क्या हुआ! इतनी प्यारी लड़की…बिलकुल तिशा…” मैंने बात को नज़रअंदाज़ करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाने की असफ़ल कोशिश की।
“बस-बस, फिर तिशा…तिशा ने ही खून पी लिया है। मुझे नहीं सुनना।” माँ ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा।
मैं कुछ कहता इससे पहले ही मौके की तलाश में बैठी हुई मेरी बहन ने सास-बहू के नाटकों की तरह आग लगाना शुरू कर दिया।
“देख रही हो, मम्मी। आजकल इन्हें लड़कियां सुंदर लगने लगी है। हाँ, हाँ भाई लगेंगी क्यों नहीं… उमर जो हो रही है।” उसके चेहरे के भाव यूं तो मुझे परेशान करने के लिए पर्याप्त थे।
किंतु आज मैं नहीं भटका। मैं और भी नाटकीय ढंग से बोला “हाँ, हाँ… क्या करूं थी ही ऐसी… त्रिपुरसुंदरी।”
“हाँ, तो लला नाम, पतो पूछ लेते।” माँ ने खिंचाई करते हुए कहा।
“माँ अअअअअ, सुनो नाम है नित्या और…।” मैंने आज का पूरा किस्सा ज्यों का त्यों माँ को सुना दिया।
सब कुछ सुनाने के बाद स्वाति ने माँ से कहा – “मम्मी, स्किन। इन्हें बड़े परफ्यूम पता हैं।”
“तुमने तैयारी फिर छोड़ दी?” माँ ने आश्चर्यचकित और उदासीन आंखों से मेरी ओर देखते हुए प्रश्न किया।
मेरे पास मम्मी की आंखों में तैर रहे इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। मैं नज़रें झुकाए खड़ा रहा। चेहरे से मुस्कुराहट जा रही थी। माँ मुझे देख रही थीं। स्वाती धीरे-धीरे इधर-उधर होने लगी। उसे पता था कि वह अगर सामने रही तो ऐसा ही कोई सवाल उससे भी पूछा जा सकता था। किंतु माँ ने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की। माँ ने हंसी छुपाते हुए बस इतना पूछा –
“नंबर भी ले लिया क्या?”
मुरझाया हुआ चेहरा फिर खिलने लगा। उगते हुए सूरज की भांति शर्म से लाल हो गया और लजाते हुए बोला – “अरे, नहीं। बस मिला ही तो हूं आज।”
“आं…हाँ…चल खाना खा ले।”
रात हो गई थी। तकरीबन साढ़े-नौ हुए होंगे। हम सभी अपने-अपने बिस्तरों में थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में पुरानी यादें घूम रही थीं। काफी अरसे बाद गुल की और ध्यान गया था। उसके साथ बीते हुए समय में अधिकतम तो मुझे अच्छा ही लगा था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे।
एल.एल.बी. का वह पहला दिन था। एकाउंट्स डिपार्टमेंट से आई-कार्ड लेकर मैं लॉ डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। मन में अनेकानेक प्रश्न गोते खा रहे थे। “पता नहीं कैसे बच्चे मिलेंगे?” “कैसे टीचर्स होंगे?” वगेरा, वगेरा। सोचते-सोचते, मैं डिपार्टमेंट में पहुँचा। पूरा डिपार्टमेंट खाली-खाली सा लग रहा था। तभी मेरा ध्यान एक कक्ष की ओर गया। कोई महाशय कुर्सी पर बैठे हुए थे और कक्षा ले रहे थे। मैंने वही अपनी कक्षा जानकर आदर सहित पूछा – “सर। एल.एल.बी. फर्स्ट सेम की क्लास यहीं चल रही है?”
उन्होंने मेरी और देखा और इशारा करते हुए कहा – “उस रूम में जाकर बैठो। वहाँ होगी।”
मैं कक्ष में जाकर बैठ गया। कक्ष में साठ-सत्तर बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। किंतु कक्षा में पूर्णतः सन्नाटे के सिवाय और कुछ नहीं था। कुछ ही देर में उन्ही महाशय ने प्रवेश किया। मैंने उठकर अभिवादन किया। उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रश्न किया –
“तुम्ही हो बस?”
मैं कोई उत्तर दे पाता इससे पहले ही दरवाजे से आवाज आई।
“मेय आई कम इन? सर! क्या एल.एल.बी. फर्स्ट सेम…।”
“हाँ, हाँ… आ जाओ।” प्रोफेसर ने कहा।
वह मेरी ही पंक्ति में मुझसे कुछ दूर आकर बैठ गई। एक मोटी… हालांकि मैं बता दूँ कि वह खुद को चबी कहती थी। किंतु शब्द बदलने से सच्चाई तो नहीं बदलती। वैसे उसके मोटापे का कारण थायराइड था किन्तु उसे चिड़ाये बिना मुझे चैन नहीं पड़ता था। मम्मी को उसकी आंखें बहुत सुंदर लगती थी। छोटी-सी नाक पर रखा हुआ गोल चश्मा मोटे-मोटे लाल गालों ने संभाला हुआ था। उस दिन की अगर बात कहूं तो मुझे वह एक मासूम-सी बच्ची लगी थी जो नर्सरी की जगह एल.एल.बी. में आ गई थी। अब क्योंकि कक्षा में सिर्फ हम दो ही थे। तो प्रोफ़ेसर ने कहा –
“दोनों यहीं मेरे सामने आकर बैठ जाओ। तुम दो ही तो हो बस।”
हम दोनों खिसक कर पास-पास बैठ गए। हम दोनों में से किसी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। मुझे ध्यान है वह हमेशा कहती थी ‘इट्स वैरी ईज़ी टॉकिंग टू यू।’
“मेरा नाम प्रशांत है और मैं तुम्हें जूरीसप्रूडेंस और टोर्ट पढ़ाऊँगा । तुम्हारे नाम क्या हैं?।”
“अनिरुद्ध”
“गुल”
“ओके। तो हम आज से ज्यूरीस शुरू करेंगे।”
कक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है अभी कुछ पंद्रह मिनट हुए होंगे। अध्यापक ने पूछा –
“तुम दोनों में से कॉमर्स किसके पास थी?”
“मेरे पास…।” हम दोनों ने एक ही सुर में कहा।
“तो तुम दोनो ने ‘लैसे फेयर’ का कांसेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा।”
“हाँ, सर बल्कि मैंने अभी दो – चार दिन पहले ही इकोनॉमिक्स में पढ़ा है।” मैंने चहकते हुए कहा।
“ठीक है तो बताओ।”
“आ… सर कुछ ऐसा है ना कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी टाइप का कुछ।”
“याद नहीं है ठीक से… सुनो”। सर ने अहस्तक्षेप नीति को पूरी तरह समझाया।
अहस्तक्षेप नीति को पूर्णतः समझाने के बाद प्रोफेसर ने हमसे नोट्स बनाने के लिए कहा। सर ने बताना करना शुरू किया ही था कि ‘लैसे फेयर’ का वर्णविन्यास ही मुझसे गलत हो गया। मेरी इस गलती को देखते हुए गुल ने कुछ खीझते हुए और मुँह सिकोड़ते हुए कहा –
“स्पेलिंग तक तो आती नहीं है, चार दिन पहले ही पढ़ा है।”
“सर सच में…।” कुछ आश्चर्य जनक मुस्कुराहट के साथ मैंने कहा।
“अरे, तो कोई बात नहीं।” प्रोफेसर ने भी हंसते हुए समझाया।
“सर, मुझे तो कॉम्प्लेक्स फ़ील हो गया ना।” गुस्सा और नाक पर लाते हुए उसने कहा।
हम दोनों उसका चेहरा देखकर हँसने लगे।
कक्षा समाप्त होने के बाद हम दोनों ने टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने का विचार बनाया। कॉलेज से ई.वी. चौक तक हम ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे जैसे कितने बरसों के बिछड़े आज मिले थे। “लैसे फेयर” ने हमारी पहली मुलाकात यादगार बना दी थी। हम दोनों भी कई बार इस बात को याद करते हुए खूब हँसते थे।
जब भी कभी वह दिन याद करता हूं तो आज भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। एक-एक करके सभी मधुर मधुर स्मृतियां नयन पटलों पर तैरने लगीं। किंतु सभी स्मृतियां मधुर तो नहीं होतीं। अचानक आँखें भर आयीं।
“बस, बस, बस अब और नहीं।” उद्वेलन भरे मन से बस इतनी आवाज आई और मैं उठकर बैठ गया। वह एक कटु स्मृति उन सभी मधुर स्मृतियां पर भारी थी। मैं उसके किए पर उसे माफ कर चुका था। किंतु फिर भी…मैंने उठकर पानी पिया और बालकॉनी में जाकर खड़ा हो गया। शरदचंद्र बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। उद्द्वेलन शांत हो गया था। आकर लेट गया, पता नहीं किस समय निद्रा ने मुझे अपनी गोद में जगह दे दी।
सुबह उठा तो आँखों में हल्की सूजन थी। ठीक से देख पाऊँ इतनी तो खुल ही रही थी। तैयार होकर पुस्तकालय की ओर चल दिया। पिछली रात की उदासी अब तक चेहरे पर थी। पुस्तकालय में घुसते ही किताबें निकाली और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। कुछ देर यूं ही किताब निहारता रहा। फिर एक गहरी सांस ली और किताब खोलकर पढ़ने में लीन हो गया। कुछ ही देर में, मैं दिव्या के दुःख के सामने अपने दुःख को अत्यंत सूक्ष्म महसूस करने लगा।
“हाए! हेलो!” किसी ने मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
मैंने उस ओर देखा, नित्या मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी किन्तु मैं एक शून्य में अटका हुआ उसे देख रहा था। उसके हाथों के इशारों ने मेरा ध्यान भंग किया।
“हेलो, नित्या।” मैंने बहुत हलकी और कुछ-कुछ बनावटी मुस्कान के साथ हाथ से अभिवादन किया।
“हाँ, हाँ…आज क्या शुरू कर रहे हो?”
“दिव्या।” मैंने किताब उसे दिखाते हुए कहा।
“ओह…यशपाल। मैं तो आज महाभोज खत्म करने की कोशिश करूंगी।”
“नाइस।” मैंने अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया।
☘☘☘
माला है एक प्रेम की, मोती भाव से जान।
एक आवत एक जात है, माला वही समान।।